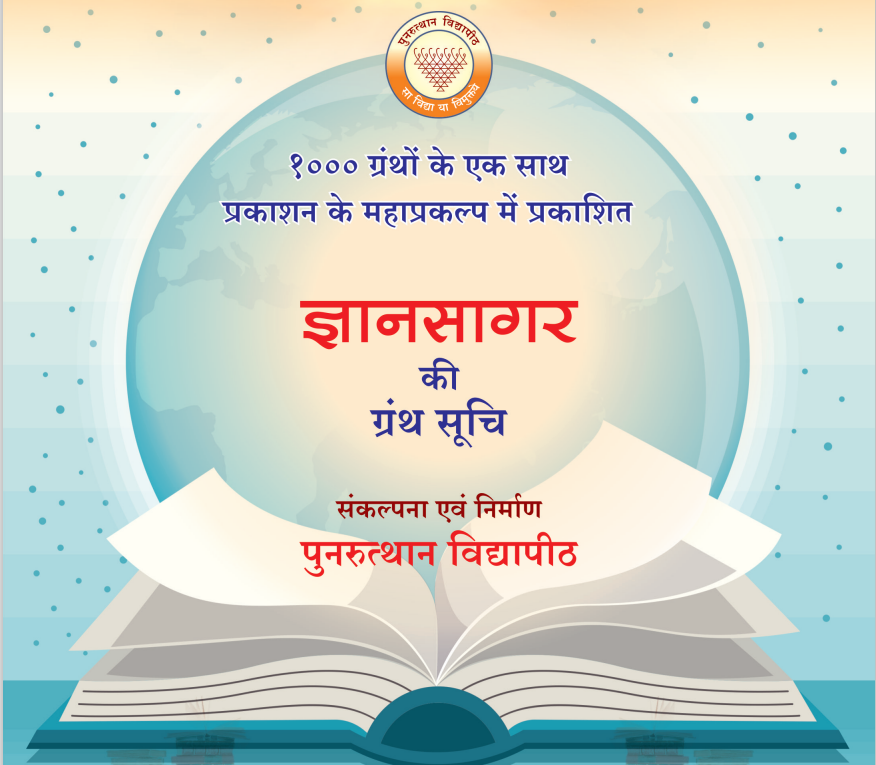भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल धारणा है कि इस जगत के मूल में एक ही तत्व है। यह मूल तत्व अव्यक्त, अचिंत्य, अकल्प्य, अदृश्य, अजर, अस्पर्शय, अमर होता है। यह सृष्टि इस मूल तत्व का व्यक्त रूप है। इस सृष्टि का मूल कारण इस तत्व का काम संकल्प “एकोsहम् बहूस्याम्” है। इस काम संकल्प की पूर्ति के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। आत्म तत्व ही चेतन और जड़ रूप में सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण बना। धर्म से इस सृष्टि को धारण किया अर्थात विश्व नियम और सृष्टि व्यवस्था बनी।
भारतीय विचार और जीवन दृष्टि में सभी व्यक्तियों अर्थात सृष्टि के सभी व्यक्त रूपों का एक ही अंतिम गंतव्य कहा गया है “इस आत्म तत्व का साक्षात्कार”। इस गंतव्य को मोक्ष पुरुषार्थ, परमात्मा में विलीन होना, कैवल्य, प्रभुचरण गमन आदि विभिन्न संज्ञाओं से व्याख्यायित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इस गंतव्य तक पहुँचने की विकास यात्रा है। आत्मतत्व से प्रारंभ होकर आत्मतत्व का साक्षात्कार हो उसमे विलीन होना, ये ही जगत का चक्रीय नियम है।
मनुष्य इस आत्म तत्व की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है क्योंकि उसे ही अंतिम गंतव्य तक पहुँचने के सभी साधन उपलब्ध हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का दायित्व और अधिकार है कि वह आवश्यक पुरुषार्थ कर इस गंतव्य तक अवश्य पँहुचे। मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य पुरुषार्थ हेतु सामर्थ्य सिद्धि है।
पुनरुत्थान विद्यापीठ ने जीवन की इस सामर्थ्य सिद्धि की यात्रा को “समग्र जीवन विकास” की यात्रा कहा है और इस दिशा में होने वाले विकास को परमेष्ठिगत विकास की संज्ञा दी है। परमेष्ठिगत विकास के अंग रूप में व्यक्ति का सृष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास के अंग रूप में व्यक्ति का समष्टिगत विकास और समष्टिगत विकास के अंग रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास अनुस्यूत है। इस प्रकार से विकास कर प्रत्येक व्यक्ति आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करता है। इस जीवन में आनंद, प्रेम, सौन्दर्य, स्वतंत्रता, सहजता का अनुभव करता है और अंतिम गंतव्य तक की यात्रा कर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
समग्र जीवन विकास एक आजीवन और सार्वत्रिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत, अतुलनीय और चक्रीय स्वरूप में सतत होती रहती है। इस प्रक्रिया को प्रत्येक व्यक्ति हेतु सरल, सहज और सफल बनाने के हेतु से समाज की शिक्षा व्यवस्था की रचना होती है। ऐसी तात्विक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा को ही सनातन, धार्मिक और भारतीय शिक्षा व्यवस्था कहा जा सकता है।
पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रतिमान विकास, निरूपण, अनुसंधान, क्रियान्वयन, प्रतिष्ठा एवं प्रसार हेतु पिछले १८ वर्षों से समर्पित और कार्यरत है।
समग्र जीवन विकास की संकल्पना
परमेष्ठिगत विकास
जब मनुष्य को आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तो उसे “अहं ब्रह्मास्मि” और “सर्व खलु इदं ब्रह्म” की अनुभूति होती है अर्थात उसे यह ज्ञान होता है कि मेरा मूल रूप और इस जगत का मूल रूप एक ही है। परमेष्ठिगत विकास का अर्थ है व्यक्ति का आत्मतत्व की अनुभूति तक का, ज्ञान, भक्ति और कर्म के आधार पर, विकास।
सृष्टिगत विकास
इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं हैं अपितु पशु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, नदी, सागर, भूमि, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब सृष्टि के ही अंश स्वरूप हैं। सृष्टि आत्मतत्व का व्यक्त रूप है, इस प्रकार से सृष्टि के प्रत्येक अंग से भी एकात्मता का अनुभव कर व्यवहार करना परमेष्ठिगत विकास के अंग रूप में सृष्टिगत विकास है।
सृष्टिगत विकास के ४ लक्षण हैं :
(१) सृष्टि आत्मतत्व का ही विस्तार है ऐसा जानना : सृष्टि के सभी अंग आत्मतत्व के ही व्यक्त रूप हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और इसी भाव से आचरण करना।
(२) सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना : मनुष्य भी इसी सृष्टि का अंग है और सृष्टि के अन्य अंगों के कारण ही उसका जीवन संभव है। सृष्टि के सभी अंगों के मनुष्य पर अनेक उपकार हैं, इसका स्मरण कर सृष्टि के सभी अंगों के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित होना।
(३) सृष्टि का शोषण नहीं, दोहन करना : सृष्टि मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता और कामना की पूर्ति का साधन है। धर्म को जानना और धर्म के अनुसार सृष्टि का दोहन करना। स्वार्थ और लालसा से प्रेरित होकर अमर्याद रूप से, आवश्यकता से अधिक छीन कर सृष्टि का शोषण करना होता है। ऐसा नहीं करना ।
(४) सृष्टि का रक्षण और पोषण करना : मनुष्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है, सामर्थ्यवान है। इस सामर्थ्य का उपयोग कर सृष्टि के सभी अंगों का रक्षण और पोषण करना, उनकी सेवा करना।
सृष्टि के प्रति प्रेम, कृतज्ञता, रक्षण और पोषण का भाव रख उसका उचित दोहन कर अपने धर्म का पालन करना ही सृष्टिगत विकास है। सृष्टि से ऐसा व्यवहार करने से सृष्टि के सभी अंग, मनुष्य के धर्म पालन हेतु उत्तर वस्तुएं प्रदान करते हैं। मनुष्य भोग्य सभी पदार्थों में रस, माधुर्य, पोषण, प्रचुरता आदि है और मनुष्य को पुष्टि, संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथ ही हिंसा, प्रदूषण, द्वेष, ईर्ष्या, शोषण जैसे संकटों का जन्म ही नहीं होगा।
समष्टिगत विकास
सृष्टि में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, वे सभी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। वे सभी अपनी अपनी पद्धति से जीवन यापन करते हैं। उनके भिन्न भिन्न स्वभाव, आकांक्षाएं, वृत्तिप्रवृत्तियाँ, गतिविधियां, वर्तन आदि भी होते हैं। अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं।
परमेष्ठिगत और सृष्टिगत विकास के अंग रूप में ये आवश्यक है कि विश्व के विभिन्न समुदायों की आपस में आत्मीयता बनी रहे। समुदायों में आत्मीयता उनके बीच सामंजस्य में परिलक्षित होती है। सामंजस्य के अभाव में वैमनस्य, ईर्ष्या, अराजकता, अव्यवस्था, तनाव, संघर्ष, हिंसा, विनाश आदि ही होगा और मनुष्यों का जीवन दुष्कर हो जाएगा। प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा और समष्टि धर्म पालन समष्टिगत व्यवहार के आधार हैं।
समष्टि का सरल अर्थ है मानव समुदाय। इस मानव समुदाय के ४ स्तर मान्य हैं – (१) परिवार (२) समाज (३) राष्ट्र और (४) विश्व। समष्टिगत विकास के भी इसी प्रकार से ४ स्तर होते हैं (१) परिवारगत विकास (२) समाजगत विकास (३) राष्ट्रगत विकास और (४) विश्वगत विकास।
परिवारगत विकास : व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों के जुड़ाव की शृंखला प्रारंभ हो जाती है। वो एक परिवार में ही जन्म लेता है। उसके माता-पिता होते हैं। माता-पिता के माध्यम से उसके अन्य संबंध जैसे भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी आदि होते हैं। माता-पिता ही उसका लालन पालन, पोषण, शिक्षण आदि करते हैं। व्यक्ति व्यवसाय, रुचि, रीति, भाषा आदि के समान व्यवहार हेतु से भी एकत्र होते हैं। प्रत्येक परिवार में सदस्यों का विशेष दायित्व और कर्तव्य होता है। परिवार का एक विशेष स्वभाव भी होता है जो सभी व्यक्तियों में परिलक्षित होता है। मनुष्य का जीवन परिवार के बिना अविचारणीय है। अतः भारतीय विचार में परिवार समष्टि की इकाई रूप में मान्य है।
परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता का निर्माण करने की कुशलता परिवारगत विकास है। परिवार के कार्यों की कुशलता होना, परिवार की रीति-रिवाजों के अनुसार व्यवहार करना, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कुशलता होना, परिवारजनों से सामंजस्य बनाने का सामर्थ्य होना, परिवार की परंपराओं के निर्वाह की कुशलता होना, परिवार के हितों को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखकर व्यवहार करना आदि परिवारगत विकास के लक्षण हैं।
समाजगत विकास: विभिन्न परिवार अनेक कारणों से जैसे व्यवस्था, व्यवसाय, भाषा, रीतियाँ, सुरक्षा आदि कारणों से एकत्र आते हैं। सम्माज में विभिन्न परिवारों के व्यक्ति भी सामाजिक संदर्भ में समान विचार और व्यवहार करते हैं। समाज के साथ समरस होना, सामाजिक दायित्व का बोध होना, समाज के प्रति सेवाभाव, समाज के अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व को देखना, सामाजिक परंपराओं का पालन एवं उचित शोधन, सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करने की कुशलता आदि समाजगत विकास का प्रथम चरण है।
समाज को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्थाएं, प्रणालियाँ, नियमावली आदि बनाए जाते हैं। इन व्यवस्थाओं का निर्माण करना, कुशलता पूर्वक निर्वाह करना, अनुशासनपूर्ण उपयोग करना आदि समाजगत विकास का द्वितीय चरण है।
राष्ट्रगत विकास : विभिन्न समुदाय जब एक जीवन दृष्टि, संस्कृति, दर्शन, सिद्धांत और सकल व्यवस्था से प्रेरित होते हैं, तो राष्ट्र का आविर्भाव होता है। राष्ट्र का अर्थ भूभाग, भौगोलिक और भौतिक गुणधर्म, उसमे निवास करने वाली प्रजा, प्रजा की जीवन दृष्टि, प्रजा के व्यवहार को प्रेरित करने वाली संस्कृति, विचारों और व्यवहारों को आधार देने वाला दर्शन, सकल व्यवस्था आदि का सम्मिलित स्वरूप है। राष्ट्र सकल मानव समुदाय की साँस्कृतिक इकाई के रूप में मान्य है।
स्वराष्ट्र के साथ समरस होना, राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान एवं आदर, राष्ट्र की व्यवस्थाओं के साथ समायोजन, परंपराओं का सम्मान और यथोचित पालन, जीवनदर्शन के अनुसार आचार-विचार एवं व्यवहार, राष्ट्रधर्म संरक्षण आदि करने की कुशलता, मानस और सामर्थ्य ही राष्ट्रगत विकास हैं।
विश्वगत विकास: इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मानव समुदाय की विश्व संज्ञा मान्य है। विश्व में अनेक राष्ट्र होते हैं। इन सबकी संस्कृतियों का ज्ञान होना, उनसे सामंजस्य और समरसता निर्माण करना, सबके प्रति सम्मान और आदर होना आदि की कुशलता, मानस और सामर्थ्य ही विश्वगत विकास है।
व्यक्तिगत विकास
व्यक्ति अर्थात आत्मतत्व का व्यक्त रूप। इस व्यक्त रूप का हेतु आत्मा द्वारा इस जगत का अनुभव प्राप्त करना है। इस व्यक्तरूप का भाव ही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तिगत विकास का अर्थ आत्मा द्वारा अनुभव और अनुभूति की सभी संभावनाओं का विकास करना है।
शास्त्रों (तैत्तरीय उपनिषद आदि) में व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु ५ आयामों का विवरण है। इन आयामों मनुष्य की आत्मा के आयाम होने के कारण से पंचआत्मा ही कहा गया है। ये पाँच आयाम हैं (१) आनंदमय आत्मा (२) विज्ञानमय आत्मा(३) मनोमय आत्मा(४) प्राणमय आत्माऔर (५) अन्न-रसमय आत्मा। सामान्य भाषा में इन्हे चित्त, बुद्धि, मन, प्राण एवं शरीर कहते हैं। इनके विकास से ही व्यक्तित्व की संभावनाओं का पूर्ण विकास संभव है। व्यक्तित्व विकास का एक प्रचलित नाम सर्वांगीण विकास भी है।
आनंदमय आत्मा की एक संज्ञा चित्त भी है। आत्मा द्वारा इस जगत की अनुभूति का पहला स्तर चित्त है। जीवन के विभिन्न अनुभव, निर्णय आदि चित्त पर संस्कार रूप में अंकित होते जाते हैं। आत्मा इन्ही संस्कारों से जगत का अनुभव करती है। शुद्ध चित्त अर्थात संस्कारों का यथार्थ परक और ज्ञानात्मक होना। शुद्ध चित्त के कारण आत्मा को आनंद, प्रेम, सौन्दर्य, स्वतंत्रता, सहजता का अनुभव होता है। चित्त शुद्धि ही आनंदमय आत्मा का विकास है।
आत्मा की अनुभूति का अगला स्तर है विज्ञानमय आत्मा। इसे सामान्य रूप से बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि ही मन द्वारा प्रस्तुत विचार को निरीक्षण-परीक्षण, संश्लेषण-विश्लेषण, तर्क-अनुमान, विवेक और निर्णय प्रक्रिया से निश्चित कर चित्त पर संस्कारों का निर्माण करती है। बुद्धि की इन प्रक्रिया सामर्थ्य का विकास कर बुद्धि को तीक्ष्ण, कुशाग्र और विशाल बनाना बुद्धि विकास है।
आत्मा की अनुभूति का अगला स्तर है मनोमय आत्मा। इस सामान्य रूप से मन भी कहते हैं। मन का स्वभाव चंचल और द्वन्द्वात्मक है। मन जगत के सभी विषयों के प्रति सदैव प्रेरित रहता है। इंद्रियजन्य ज्ञान को द्वन्द्वात्मक विचार में परिवर्तत कर, बुद्धि द्वारा उचित संस्कार हेतु प्रस्तुत करता है। मन को शांत कर, एकाग्र कर उसको शुद्ध चित्त से, बुद्धि के नियंत्रण द्वारा विवेकपूर्ण रूप मे केवल यथोचित विषयों मे प्रेरित करना ही मनोमय आत्मा का विकास है।
आत्मा की अनुभूति का अगला स्तर प्राण है। प्राण ही जीवनी शक्ति है अर्थात प्राण ही मन के आदेश पर इंद्रियों को प्रेरित और संचालित करता है। प्राण ही इंद्रियजन्य ज्ञान को मन के विचार हेतु प्रस्तुत करता है। प्राण ही मन की विचार शक्ति और शरीर की क्रिया शक्ति है। प्राण के द्वारा ही मन का विभिन्न विषयों में प्रवेश संभव है। प्राण की चार प्रवृत्तियाँ है – आहार, निद्रा, भय और मैथुन। प्राणमय आत्मा के विकास का अर्थ शारीरिक मर्यादाओं की सीमा का विस्तार है। प्राणों का बलवान, एकाग्र और प्रवृत्तियों में संतुलित होना ही प्राणों का विकास है।
आत्मा की अनुभूति का अंतिम स्तर अन्नमय आत्मा है। इसे सामान्य भाषा में शरीर कहा जाता है। पंचमहाभूत निर्मित शरीर एक यंत्र की भांति है। प्राण की शक्ति से और मन की प्रेरणा से शरीर कार्य करता है और इस जगत की विभिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त रहता है। शरीर ही आत्मा के अनुभवों की मर्यादा है। शरीर का स्वस्थ, निरामय, बलवान, ओजपूर्ण, सहनशील, लौचिक और सुडौल होना ही अन्न-रसमय आत्मा का विकास है।